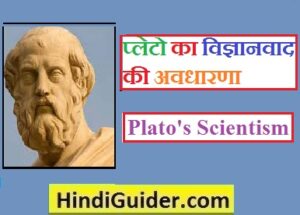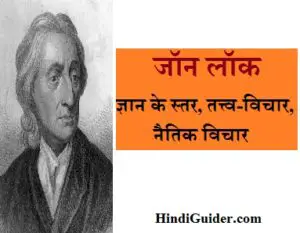धर्म का अर्थ
धर्म-दर्शन के स्वरूप और क्षेत्र को भलीभाँति समझने के लिए सर्वप्रथम धर्म और दर्शन का अर्थ समझना आवश्यक है। ‘धर्म’ शब्द हम सब के लिए एक ऐसा परिचित शब्द है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति इस शब्द के अर्थ के विषय में कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं करता। यदि उससे पूछा जाए कि धर्म क्या है तो संभवतः वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म आदि की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए इस शब्द का अर्थ स्पष्ट करेगा और हमें बताएगा कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि उपासना-स्थलों में जाकर विशेष प्रकार से प्रार्थना या पूजा करना ही धर्म है। साधारण व्यक्ति जब ‘धर्म’ शब्द सुनता या पढ़ता है अथवा स्वयं इस शब्द का प्रयोग करता है तो प्रायः उसके मन में किसी विशेष उपासना-स्थल, उसमें विशेष प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्तियों, जन्म, नामकरण, विवाह, मत्य आदि महत्त्वपूर्ण अवसरों पर संपन्न किए जाने वाले विशेष कृत्यों या अनुष्ठानों तथा विशेष प्रकार के वस्त्र पहने हुए ऐसे व्यक्तियों का चित्र उभरता है जिन्हें ‘साधु’ या ‘संत’ कहा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति ‘धर्म’ शब्द को कुछ विशेष बाहय वस्तओं, भवनों, वस्त्रों, पुस्तकों, व्यक्तियों तथा प्रार्थना या पूजा-पाठ संबंधी कर्मकांड से ही जोड़ता है।
यद्यपि धर्म का उपर्युक्त प्रचलित सामान्य अर्थ दार्शनिक दृष्टि से बहत संतोषप्रद नहीं है फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसमें आंशिक सत्य अवश्य विद्यमान है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विशेष उपासना-स्थल, पवित्र ग्रंथ, प्रार्थना अथवा पूजा-पाठ संबंधी कर्मकांड तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान धर्म के महत्त्वपूर्ण अंग माने जाते हैं जिन्हें हम धर्म का ‘बाह्य पक्ष’ कह सकते हैं। जनसाधारण धर्म के इस बाहय पक्ष को अत्यधिक महत्त्व देता है। और इसी के आधार पर धर्म को अन्य सभी विषयों, विचारों तथा सिद्धांतों से पृथक करता। है। ऐसी स्थिति में धर्म का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके इस बाहय पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रायः सभी धर्मों में धर्म का यह बाह्य पक्ष अनिवार्यतः विद्यमान रहता है।
जिसके द्वारा उन्हें एक-दसरे से पृथक किया जाता है और जिसके कारण प्रत्येक धर्म के अनुयाई अपने आपको अन्य सभी धर्मों के अनुयाइयों से भिन्न मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न धर्मों के कर्मकांड संबंधी बाह्य पक्ष में पर्याप्त भिन्नता होती है जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करती है और जो उनके अनुयाइयों में पारस्परिक विद्वेष तथा संघर्ष का प्रमुख कारण बनती है। परंतु इसके साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि धर्मों में उक्त भिन्नता के होते हुए भी हम सभी धमा के लिए एक ही शब्द ‘धर्म’ का प्रयोग करते हैं
दर्शन का अर्थ
धर्म के स्वरूप की विवेचना करने के पश्चात अन्न दर्शन के अर्थ पर भी विचार करना आवश्यक है जिससे धर्म-दर्शन के स्वरूप को भलीभाँति स्पष्ट किया जा सके। धर्म के समान ही दर्शन की भी ठीक-ठीक और सर्वमान्य परिभाषा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग भी भिन्न-भिन्न अर्थों में किया जाता है। सामान्य व्यक्ति ‘धर्म’ शब्द का अर्थ तो कुछ सीमा तक समझता है और हम देख चुके हैं कि इस अर्थ में आंशिक सत्य भी विद्यमान है; कितु ‘दर्शन’ शब्द का अर्थ उसे बहुत ही अस्पष्ट प्रतीत होता है जिसके कारण वह इसके संबंध में अपनी कोई निश्चित अवधारणा नहीं बना पाता। जब वह ‘दर्शन’-शब्द पढ़ता या सनता है तो सामान्यतः उसके मन में कुछ ऐसी बातों का विचार आता है जिनका संबंध ईश्वर, आत्मा आदि अलौकिक आध्यात्मिक सत्ताओं से है और जो अत्यंत कठिन होने के कारण उसकी समझ से परे हैं। दर्शन के विषय में जनसाधारण की यही अवधारणा इस भ्रामक विचार को जन्म देती है कि दर्शन एक ऐसा कठिन बौद्धिक विषय है जिसका मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध नहीं है।
दर्शन निश्चय ही बौद्धिक विषय है और अपेक्षाकृत कुछ कठिन भी है, किंत इसे अलौकिक आध्यात्मिक सत्ताओं तक ही सीमित तथा मानव जावन से पृथक या असंबंद्ध मानना भामक है। वास्तव में साहित्य के समान ही दर्शन भी मनुष्य के जीवन से प्रत्यक्षतः संबंधित है. क्योंकि इन दोनों की विषयवस्तु मानव-जीवन की शाश्वत मूल समस्याएं हैं। इन दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि साहित्य का प्रधान तत्व भावना है जबकि दर्शन का मख्य तत्त्व विचार या तर्क है।
दर्शन ‘संस्कृत’ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ‘देखना या खोजना’। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से ‘दर्शन’ का अर्थ है ‘सत्य का अनुसंधान’ अथवा सत्य की खोज। जो निष्पक्ष विचार एवं तर्क के आधार पर जीवन के मूल सत्यों का अनुसंधान करता है वही दर्शन है। दर्शन के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रचलित ‘फिलॉसॉफ़ी’ शब्द का भी लगभग यही अर्थ है। इस शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के ‘फिलॉसॉफ़ॉस’ तथा ‘सोफिया’ इन दो शब्दों से हई है जिनका अर्थ क्रमशः ‘प्रेम’ और ‘ज्ञान’ अथवा ‘विद्या’ है। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से ‘फिलॉसॉफी का अर्थ है ‘विद्यानराग’ या ‘जान के प्रति प्रेम’। इस अर्थ से भी यही ध्वनित होता है कि ‘फिलॉसॉफी’ जीवन के शाश्वत मल सत्यों के ज्ञान के प्रति अनुराग है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ‘दर्शन’ तथा ‘फिलॉसॉफी’ दोनों शब्दों के अर्थ में ज्ञान अथवा चितन विषयक तत्त्व की प्रधानता है और यही दर्शन का मूल तत्त्व भी है।
दर्शन के अर्थ को भलीभाँति स्पष्ट करने के लिए उसके उपर्युक्त बौद्धिक तत्त्व पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यही तत्त्व उसे साहित्य, कला, धर्म आदि कुछ अन्य विषयों से पृथक करता है। वस्तुतः दर्शन की वही परिभाषा संतोषप्रद मानी जा सकती है जिसमें उसके इस चिंतन-प्रधान बौद्धिक तत्त्व को समुचित स्थान दिया गया हो। यद्यपि दर्शन की कोई ऐसी परिभाषा देना बहत कठिन है जो सर्वमान्य हो और जिसे सभी दृष्टियों से संतोषप्रद माना जा सके, फिर भी दर्शन की मूल विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए हम उसकी निम्नलिखित परिभाषा दे सकते हैं-दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित मूल तत्त्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि दर्शन मनुुष्य की वह विशुद्ध बौद्धिक क्रिया है जिसमें निष्पक्ष चितन, तर्क और विश्लेषण का सर्वप्रमख स्थान होता है। अब हम संक्षेप में दर्शन के उन महत्त्वपूर्ण तत्त्वों की व्याख्या करेंगे जिनकी ओर उपर्युक्त परिभाषा में संकेत किया गया है।
(1). दर्शन के स्वरूप को भलीभाँति समझने के लिए सर्वप्रथम इस तथ्य की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि दर्शन का मूल आधार मनुष्य की तर्कबुद्धि अथवा विवेक-शक्ति ही है। मानवीय संवेगों या भावनाओं का दर्शन में कोई स्थान नहीं है। जब दार्शनिक किसी विषय की निष्पक्ष व्याख्या अथवा विवेचना करता है तो वह भावनाओं या संवेगों से पूर्णतः मुक्त होकर केवल अपनी तर्कबुद्धि पर निर्भर रहता है। यदि कोई दार्शनिक किसी विषय की विवेचना करते समय अपने संवेगों या पूर्वाग्रहों से प्रभावित होता है तो निष्पक्ष न होने के कारण उसकी इस विवेचना का दार्शनिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि दर्शन का यह विशद्ध बौद्धिक पक्ष उसे उन सभी विषयों से पृथक करता है जिनमें भावनाओं. संवेगों या अभिवत्तियों की प्रधानता होती है। इन विषयों में साहित्य, कला, धर्म आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी विषयों के विपरीत दर्शन निष्पक्ष रूप से पर्णतः तर्क का ही अनसरण करता है-फिर चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। इस प्रकार विशुद्ध बौद्धिकता अथवा तार्किकता दर्शन की अनिवार्य मूल विशेषता है।
(2) दर्शन की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसका अत्यधिक व्यापक क्षेत्र। दर्शन किसी भी विषय अथवा समस्या के मूल तत्त्वों या उसकी आधारभूत मान्यताओं का निष्पक्ष रूप में विश्लेषण कर सकता है: उसका क्षेत्र किसी एक विषय अथवा समस्या तक सीमित नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक विषय की कुछ आधारभत मान्यताएँ होती हैं जिन्हें वह बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है और जिन पर उसका अस्तित्व एवं संपूर्ण विकास निर्भर होता है। साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म, राजनीति, समाज, इतिहास, कानून आदि सभी विषयों के संबंध में यही बात कही जा सकती है। किसी विषय की ये मूलभूत मान्यताएँ कहाँ तक सत्य एवं तर्कसंगत हैं इस प्रश्न के समचित उत्तर पर ही वास्तव में उसका महत्त्व निर्भर है और दशन इसी प्रश्न का निष्पक्ष रूप से उत्तर देने का प्रयास करता है। दर्शन ही हमें यह बताता है कि किस विषय की कौन-सी आधारभत मान्यताएँ सत्य हैं और कौन-सी मिथ्या। यही कारण है कि दर्शन का संबंध किसी एक विषय के साथ न होकर सभी विषयों के साथ है। संसार में ऐसा कोई महत्त्वपर्ण विषय नहीं है जो दर्शन से असंबद्ध हो और जिसे दर्शन की सहायता की आवश्यकता न पड़ती हो। ‘साहित्य-दर्शन’, ‘विज्ञान-दर्शन’, ‘कला-दर्शन’ ‘धर्म-दर्शन’, ‘राजनीति-दर्शन’, ‘समाज-दर्शन’, ‘इतिहास-दर्शन’, ‘कानून-दर्शन’ आदि। इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हैं। इन सभी विषयों के लिए दर्शन अनिवार्य है, क्योंकि वही इनकी आधारभूत मान्यताओं के सत्य अथवा मिथ्या होने की निष्पक्ष परीक्षा करता है। इसी कारण बहुत प्राचीन काल से ही दर्शन को समस्त ‘विज्ञानों का विज्ञान’ माना जाता रहा है और आज भी किसी विषय की उच्चतम उपाधि को डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफीया ‘पी-एच०डी०’ कहा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि संसार के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषय के साथ वह अनिवार्यतः संबद्ध रहता है।
(3) किसी भी विषय से संबंधित विश्वासों अथवा मान्यताओं को स्वीकार या अस्वीकार करने से पूर्व उनकी निष्पक्ष रूप से आलोचनात्मक परीक्षा करना दर्शन की तीसरी अनिवार्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो उसे अन्य सभी विषयों से पृथक करती है। दार्शनिक किसी विश्वास अथवा मान्यता को तब तक स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता जब तक वह सभी प्रासंगिक तथ्यों और समुचित प्रमाणों के आधार पर उसकी भलीभाँति आलोचनात्मक परीक्षा नहीं कर लेता। इस प्रकार की निष्पक्ष आलोचनात्मक परीक्षा के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना प्रत्येक विचारक या दार्शनिक का अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। संक्षेप में ये नियम निम्नलिखित है:-
(क) स्पष्टता का नियम :
किसी भी विश्वास या सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करने के लिए सर्वप्रथम उन शब्दों तथा अवधारणाओं का ठीक-ठीक अर्थ समझना आवश्यक है जिनके माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ यदि हम ईश्वर, आत्मा, ‘आस्था’, ‘श्रति’. ‘ज्ञान’ आदि शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ नहीं समझते तो हमारे लिए इनसे संबंधित सिद्धांतों और मान्यताओं की आलोचनात्मक परीक्षा करना समय नहीं है। इसी कारण समकालीन दर्शन में सभी महत्त्वपर्ण विषयों से संबंधित भाषा के समचित विश्लेषण को बहुत महत्त्व दिया जा रहा है। वस्तुतः किसा आलोचनात्मक परीक्षा के लिए उसे अभिव्यक्त करने वाली भाषा का भलीभाति विश्लेण करके उसके अर्थ को स्पष्ट करना अनिवार्य है।
(ख) संगति का नियम :
जब कोई व्यक्ति किसी विशेष सिद्धांत या विश्वास को स्वीकार का दावा करता है तो दार्शनिक के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि उसके विचारों में संगति है अथवा नहीं। ऐसा कोई भी विश्वास या सिद्धांत तर्कसंगत नहीं हो सकता जिसमें स्वतोव्याघात विद्यमान है-अर्थात जिसकी मान्यताओं में परस्पर विरोध है। इसका कारण यह है कि उसकी परस्पर विरोधी मान्यताएँ हमारे लिए उसे निरर्थक बना देती हैं। उदाहरणार्थ किसी घातक रोग से ग्रस्त होने पर यदि कोई व्यक्ति एक ओर तो यह कहता है कि ईश्वर की उपासना करने से वह पर्णतः स्वस्थ हो जाएगा और दूसरी और वह योग्य चिकित्सकों का परामर्श लेता है तथा उनके द्वारा दी गई औषधियों का सेवन भी करता है तो यह स्पष्ट है कि उसके विचारों में गंभीर असंगति अथवा स्वतोव्याघात विद्यमान है। यह असंगति उसके विचारों को तर्कहीन और निरर्थक बना देती है, क्योंकि रोग-मुक्त होने के लिए वह ‘ईश्वरोपासना के प्रभाव तथा चिकित्सा-विज्ञान की क्षमता इन दोनों परस्पर विरोधी विश्वासों को एक साथ स्वीकार करता है। ऐसे स्वतोव्याघातपर्ण विचार या सिद्धांत कभी भी सत्य और तर्कसंगत नहीं हो सकते। इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से केवल उन्हीं विश्वासों, विचारों या सिद्धांतों को सत्य माना जा सकता है जो स्वतोव्याघात से पूर्णतः मुक्त हों-अर्थात् जिनमें संगति विद्यमान हो।
(ग) तथ्यों की खोज और स्वीकृति का नियम :
किसी विश्वास अथवा सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करने के लिए यह अनिवार्य है कि उससे संबंधित सभी तथ्यों को खोजा जाए और उन्हें ध्यान में रखते हुए उसके सत्य या मिथ्या होने का निर्णय किया जाए। इस संबंध में किसी ऐसे प्रासंगिक तथ्य की उपेक्षा करना जो हमारे सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण हमें अप्रिय है उसकी आलोचनात्मक परीक्षा में निश्चय ही बाधक होगा। परंत इस प्रकार की परीक्षा के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को खोजना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें बिना किसी संकोच के स्वीकार करना और समुचित महत्त्व देना भी आवश्यक है। मनष्य की यह स्वाभाविक दुर्बलता है कि वह जानबूझ कर ऐसे तथ्यों को प्रायः अस्वीकार करता है जो उसके विश्वास या सिद्धांत का खंडन करते हैं। परंतु दार्शनिक के लिए इस दर्बलता से पर्णत भक्त होना बहत आवश्यक है, अन्यथा वह निष्पक्ष आलोचक होने के अपने गंभीर दायित्व की कभी पूर्ति नहीं कर सकता।
वस्तुतः किसी विश्वास या सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षा करते समय उससे संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों को खोजना और पूर्णतः तटस्थ एवं ‘निष्पक्ष होकर उन्हें स्वीकार करना तथा समचित महत्त्व देना दार्शनिक का अनिवार्य कर्तव्य है। समस्त प्रासंगिक तथ्यों की निष्पक्ष खोज तथा समुचित स्वीकृति के कारण उपर्यक्त नियम को ‘निष्पक्षता का नियम’ भी कहा जा सकता है। इस नियम के अनुरूप कार्य करके ही दार्शनिक अपने दायित्व की पूर्ति कर सकता है।
(घ) प्रमाणों की अनिवार्यता का नियम :
किसी भी विचार, विश्वास, मान्यता अथवा सिद्धांत को सत्य मानने से पर्व उस के समर्थन में पर्याप्त एवं समुचित प्रमाणों की खोज करना दार्शनिक के लिए अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि केवल पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण ही वास्तव में किसी मान्यता, सिद्धांत या विश्वास को सत्य अथवा मिथ्या प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसे प्रत्येक विश्वास अथवा सिद्धांत की सत्यता संदिग्ध ही मानी जा सकती है जिसकी पुष्टि के लिए हमारे पास कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। किसी भी विश्वास या सिद्धांत के सत्य अथवा मिथ्या होने के संबंध में हमारे लिए अपना निश्चित निर्णय तब तक स्थगित रखना आवश्यक हो जाता है जब तक उसके पक्ष या विपक्ष में हमें स्पष्ट, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाते। प्रमाणों की मांग करने का यहा नियम दार्शनिक को सभी प्रकर के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर किसी मान्यता, विश्वास अथवा सिद्धांत की सत्यता या प्रामाणिकता के विषय में तर्कसंगत रूप से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।
इसी नियम के आधार पर हम प्रामाणिक सिद्धांतों को सभी प्रकार के अंधविश्वास से पृथक कर सकते हैं जो प्रमाणित न हो सकने के कारण पूर्णतः मिथ्या होते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह नियम तथ्यों की खोज तथा स्वीकृति से संबंधित उपर्यक्त तीसरे नियम के साथ अनिवार्यतः संबद्ध है। इसका कारण यह है कि किसी सिद्धांत या विश्वास के सत्य अथवा मिथ्या होने के प्रमाण उससे संबंधित प्रासंगिक तथ्यों से ही प्राप्त हो सकते है। इसी प्रकार संगति संबधी दूसरे नियम का भी प्रमाण विषयक चौथे नियम के साथ अनिवार्य संबंध है, क्योंकि, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, किसी सिद्धांत में असंगति या स्वतोव्याघात का होना उसे अप्रामाणिक बना देता है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी नियमों का भलीभाँति पालन करके ही दार्शनिक किसी विश्वास अथवा सिद्धांत की निष्पक्ष आलोचनात्मक परीक्षा कर सकता है जो दर्शन का मुख्य कार्य है।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि किसी विषय के सूक्ष्म विश्लेषण तथा निष्पक्ष मूल्यांकन के रूप में दर्शन मानव-ज्ञान के सभी महत्त्वपर्ण विषयों से संबंधित है और इस दृष्टि से उसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। परंतु इसके साथ ही दर्शन मानव-जीवन की कुछ ऐसी मूल समस्याओं की भी गंभीर विवेचना करता है जो केवल उसी के क्षेत्र में आती हैं और जिनकी विवेचना अन्य कोई विज्ञान या शास्त्र नहीं करता। ये वे समस्याएँ हैं जिनका संबंध ब्रह्मांड की रचना और अंतिम सत्ता, उसके रचयिता तथा उसके विकास का लक्ष्य, ज्ञान का स्वरूप एवं प्रमाणीकरण, मानव-जीवन का परम ध्येय तथा मानवीय आचरण का मानदंड, निष्पक्ष चिंतन एवं तर्कना के मूल सिद्धांत, सौंदर्य का स्वरूप तथा सौंदर्यात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति के साधन आदि विषयों से है। इन सभी विषयों का विस्तृत विवेचन तत्त्वमीमांसा, ज्ञानमीमांसा, नीतिशास्त्र, तर्कशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र आदि दर्शन की प्रमुख शाखाओं में किया जाता है। इसी कारण उक्त सभी विषयों को दर्शन के मूल विषय माना जाता है और इन विषयों के अंतर्गत जिन समस्याओं की विवेचना की जाती है उन्हें दर्शन की आधारभूत समस्याएँ कहा जा सकता है।
प्राचीन काल से वर्तमान यग तक दर्शन के दीर्घकालीन इतिहास में महान दार्शनिकों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रश्नों से दर्शन की उपयुक्त आधारभूत समस्याओं के स्वरूप को कुछ सीमा तक समझा जा सकता है-इस ब्रहमांड की रचना कैसे, क्यों और किसके द्वारा की गई है? इसकी अंतिम सत्ता का स्वरूप क्या है? क्या यह अंतिम सत्ता निर्जीव पद्गल है अथवा क्या यह कोई चेतनापूर्ण आध्यात्मिक शक्ति है ? यदि इस बहमांड का कोई रचयिता है तो इसका स्वरूप क्या है ? क्या उसने किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए इसकी रचना की है ? क्या वास्तव में ईश्वर तथा आत्मा का अस्तित्व है और यदि इनका अस्तित्व है तो इनका वास्तविक स्वरूप क्या है ? क्या मनष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर के साथ ही उसका जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाता है अथवा क्या मृत्यु के उपरांत भी किसी अन्य रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है? क्या दिक् और काल की वस्तुगत एवं स्वतंत्र सत्ता है।
अथवा क्या मनुष्य ने केवल अपनी सविधा के लिए इन प्रत्ययों की रचना की है? मानव-जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और इसकी प्राप्ति किस प्रकार संभव है? क्या इस संसार में सचमुच ‘अच्छाई’ और ‘बुराई’ है? अथवा क्या ‘अच्छाई’ और ‘बुराई’ केवल परिस्थिति-सापेक्ष शब्द मात्र हैं? हम किस मानदंड के आधार पर मानवीय आचरण को शुभ या अशुभ कह सकते हैं और इस मानदंड के औचित्य की परीक्षा कैसे की जा सकती है? मनुष्य इस संसार में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसे प्रमाणित करने के लिए किस प्रकार के प्रमाण दिए जा सकते हैं ? सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप क्या है और हम किस मानदंड के आधार पर किसी व्यक्ति तथा वस्तु को सुंदर या कुरूप कह सकते हैं?
क्या सौंदर्य बाह्य वस्तुओं में विद्यमान रहता है अथवा क्या यह मनुष्य की अपनी दृष्टि पर ही निर्भर है? हमारे चिंतन के आधारभूत नियम क्या हैं और हम किन मानदंडों द्वारा अपने तर्कों की प्रामाणिकता का निर्णय कर सकते हैं? क्या इस विश्व में कोई निश्चित व्यवस्था और कारण-कार्य संबंधी अनिवार्य नियम है अथवा क्या इसमें घटित होने वाली समस्त घटनाएँ केवल संयोग के परिणामस्वरूप ही घटित होती हैं ? ये सभी तथा इसी प्रकार के अनेक प्रश्न दर्शन के मूल प्रश्न हैं जिन पर विश्व के महान दार्शनिक प्राचीन काल से गंभीरतापर्वक विचार करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं।
संसार के विभिन्न दार्शनिकों द्वारा शताब्दियों के निरंतर विचार-विमर्श के पश्चात् भी इन प्रश्नों का कोई स्पष्ट, निश्चित एवं सर्वमान्य उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका है। इसी कारण इन प्रश्नों को ‘दर्शन के शाश्वत प्रश्न’ भी कहा जाता है। इन शाश्वत प्रश्नों पर व्यवस्थित रूप से विचार करना और इन के समचित एवं तर्कसंगत उत्तर खोजने का प्रयास करना मख्यत दर्शन का ही कार्य है जो उसे अन्य सभी विज्ञानों तथा शास्त्रों से पृथक करता है। दर्शन के इन मल प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि मानव-जीवन तथा संपूर्ण ब्रहमांड की सभी आधारभूत समस्याओं पर इसके अंतर्गत विचार किया जाता है और यह तथ्य इसके क्षेत्र को अत्यधिक व्यापक बना देता है।
दर्शन विषयक उपर्युक्त शाश्वत प्रश्नों से हमारे इस कथन की भी पुष्टि होती है कि साहित्य के समान ही दर्शन का भी मानव-जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। वस्ततः यह कहना अनुचित न होगा कि मनुष्य का संपूर्ण जीवन भावना और विचार इन दो मूल तत्त्वों द्वारा शासित होता है जो क्रमशः साहित्य तथा दर्शन के आधारभूत तत्त्व हैं। मनुष्य के हृदय की गहरी अनुभति से साहित्य का और उसकी तर्कबुद्धि से दर्शन का जन्म होता है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, करुणा, भय, क्रोध, घृणा आदि संवेगों का अनुभव किए बिना नहीं रह सकता उसी प्रकार वह नितांत विचार शून्य जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता। यदि मनुष्य सवेगों या भावनाओं तक ही सीमित रहता है तो उसमें तथा अन्य प्राणियों में कोई अंतर नहीं रह जाता।
इसी कारण भारतीय मनीषियों ने यह कहा है कि आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन की दृष्टि से मनुष्य और पशु समान ही हैं, किंतु विवेक ही वह मूल तत्त्व है जो उसे अन्य सभी प्राणियों से पृथक करता है। हम देख चुके हैं कि मनुष्य का यह विवेक अथवा विचार ही दर्शन का मूल आधार है जिसके बिना वह वास्तविक अर्थ में ‘मनुष्य’ कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। विचार करना मनष्य का स्वाभाविक गुण है। जो उसे अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट बनाता है। वस्तुतः उसके इसी स्वाभाविक गण के कारण महान विचारकों ने उसे बौद्धिक प्राणी’ की संज्ञा दी है। दर्शन और विज्ञान दोनों ही मनुष्य के इसी स्वाभाविक गुण-अर्थात् उसकी विवेक-शक्ति-के परिणाम हैं।
जब भी कोई व्यक्ति जीवन तथा जगत् के विषय में विचार करता है और पूर्वोल्लिखित प्रश्नों में से कुछ प्रश्न उठाता है तो ‘दर्शन’ शब्द के व्यापक अर्थ में उसे ‘दार्शनिक’ कहा जा सकता है-फिर चाहे वह स्वयं इस तथ्य से परिचित हो या न हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ असाधारण परिस्थितियों के फलस्वरूप कभी न कभी इस व्यापक अर्थ में ‘दार्शनिक’ बनने के लिए बाध्य हो जाता है। उदाहरणार्थ जब उसके किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु होती है तो वह सोचने लगता है कि आखिर मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है-क्या वह सदा के लिए समाप्त हो जाता है अथवा क्या किसी अन्य रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है ?
इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति पर कोई भयंकर विपत्ति आती है तो वह प्रायः यह प्रश्न करता है कि आखिर उसे ही यह घोर यातना क्यों भोगनी पड़ रही है-उसने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उसे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है? इतना ही नहीं, कभी-कभी सामान्य परिस्थितियों में भी मनुष्य यह सोचने लगता है कि आखिर वह क्यों जी रहा है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, वह इस संसार में कहाँ से आया है और मृत्यु के पश्चात कहाँ जाएगा। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, ये तथा ऐसे ही अन्य सभी प्रश्न दर्शन के मूल प्रश्न हैं जिन पर केवल दार्शनिक ही नहीं, अपितु साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी न कभी विचार करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि सोचना मनुष्य की नियति है जिससे वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दर्शन मनुष्य से दूर और उसके लिए कोई अनजानी वस्तु न होकर वास्तव में उसके जीवन का अभिन्न अंग है।
दर्शन के संबंध में प्रायः यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि इसका आरंभ क्यों और कैसे हआ। ऊपर दर्शन के जिन मल प्रश्नों का उल्लेख किया गया है उनके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। इन प्रश्नों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य में जगत और जीवन को जानने की जो प्रबल स्वाभाविक प्रवत्ति है उसी के फलस्वरूप दर्शन का आरंभ हआ है। जब से इस पृथ्वी पर विवेकशील प्राणी के रूप में मनुष्य का विकास हुआ है तभी से वह अपने चतुर्दिक परिवेश तथा उसमें विद्यमान सभी वस्तुओं एवं प्राणियों के संबंध में अधिकाधिक जानने का प्रयास करता रहा है। प्रारंभ से ही मनष्य में यह जानने की प्रबल जिज्ञासा रही है कि वह अपने चारों ओर जिन ग्रह-नक्षत्रों, वस्तओं तथा प्राणियों को देखता है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है।
यह जिज्ञासा मानव की जन्मजात प्रवृत्ति है जो उसे स्वयं अपने विषय में तथा अपने संपर्ण परिवेश के संबंध में अधिकाधिक जानने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। वस्तुतः मनुष्य की इस नैसर्गिक अदम्य जिज्ञासा ने ही दर्शन तथा विज्ञान दोनों को जन्म दिया है और इसी जिज्ञासा के कारण इन दोनों का निरंतर विकास भी हुआ है। इस स्वाभाविक जिज्ञासा के परिणामस्वरूप मनुष्य ने जगत और जीवन का जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे उसके दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हुई है। सर्वप्रथम इस ज्ञान के कारण उसे वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझने का संतोष प्राप्त हुआ है और इस प्रकार जीवन तथा जगत् को जानने की उसकी प्रबल इच्छा की पूर्ति हुई है। दर्शन ने मुख्यतः मनष्य के इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायता की है। स्पष्ट है कि इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली जिज्ञासा को हम किसी अन्य लक्ष्य की प्राप्ति का साधन न मानकर अपने आप में साध्य मान सकते हैं। दर्शन की उत्पत्ति के मूल में मनुष्य की यही स्वतः साध्य जिज्ञासा रही है।
परंतु इसके साथ ही मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा के फलस्वरूप ऐसा ज्ञान भी प्राप्त किया है जिस ने उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसके जीवन को अधिक सुखमय बनाया है। इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य आदि-काल से ही उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है जो उसके जीवन के लिए घातक अथवा कष्टप्रद रही हैं। स्वयं अपने जीवन के लिए अपने परिवेश को अधिक सुखद बनाने का उसका यह प्रयास आज भी चल रहा है और निश्चय ही तब तक चलता रहेगा जब तक वह इस संसार में जीवित है। विज्ञान ने-जिसका जन्म भी मनुष्य की जिज्ञासा के फलस्वरूप ही हआ है-उसके इस प्रयास में विशेष रूप से सहायता दी है। इसी कारण विज्ञान दर्शन की अपेक्षा मनुष्य के व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी प्रतीत होता है। परंतु विशद्ध विज्ञान के रूप में वह भी दर्शन के समान ही मूलतः सैद्धांतिक ज्ञान है जिसका उद्देश्य जीवन और जगत के संबंध में मानव की नैसर्गिक अदम्य जिज्ञासा को शांत करना ही है। इस दष्टि से दर्शन तथा विज्ञान में आधारभत समानता है, क्योंकि दोनों का मूल स्रोत मनूष्य की जिज्ञासा ही है और दोनों में भावना की अपेक्षा तर्क को कहीं अधिक महत्त्व दिया जाता है।
परंतू यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दर्शन तथा विज्ञान का यह बौद्धिक तत्त्व इन दोनों को धर्म से पृथक करता है जिसमें तर्क की अपेक्षा भावना का ही अधिक महत्त्व होता है। धर्म तथा विज्ञान में विद्यमान मूल भेद पर यथास्थान आगे विचार किया जाएगा: यहाँ संक्षेप में धर्म और दर्शन में पाए जाने वाले अंतर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। धर्म तथा दर्शन के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही मानव-जीवन के बहुत महत्त्वपर्ण पक्ष हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य के आचरण तथा विचारों पर इन दोनों का बहत गहरा और व्यापक प्रभाव रहा है। दोनों ही मानव-जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित न होकर उसके सभी महत्त्वपर्ण पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करते रहे हैं। अतः इस दृष्टि से दोनों में पर्याप्त समानता है। परंतु इस समानता के होते हुए भी जीवन और जगत के प्रति धर्म तथा दर्शन के दृष्टिकोण में आधारभूत अंतर है जिसे स्पष्ट रूप से जान लेना बहत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि धर्म और दर्शन के मूल भेद को भलीभाँति जान लेने पर हम इन दोनों के स्वरूप को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम देख चुके हैं कि धर्म जीवन और जगत के प्रति मनुष्य की एक विशेष प्रकार की अभिवृत्ति है।
स्पष्टतः इसका अर्थ यही है कि धर्म में भावना अथवा अनुभति का ही सर्वाधिक महत्त्व होता है। इसके विपरीत दर्शन जीवन तथा जगत को समझने का मनुष्य का सुव्यवस्थित, संगतिपूर्ण और बौद्धिक प्रयास है जिसका मूल आधार भावना न होकर केवल तर्क है। भक्त या धर्मपरायण व्यक्ति केवल अपनी आस्था के फलस्वरूप अपने आराध्यं विषय के प्रति अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित करता है, इस आत्म-समर्पण के लिए वह किसी प्रकार के तर्क अथवा प्रमाण की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता। परंतु दार्शनिक किसी भी सिद्धांत, विश्वास या मान्यता को स्वीकार करने से पूर्व उसके समर्थन में पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रमाणों की माँग करता है, क्योंकि ऐसे प्रमाणों के अभाव में वह अपना कोई निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता।
इस प्रकार स्पष्ट है कि धर्म के आधारभूत तत्त्व अनुभूति और आस्था हैं जबकि दर्शन के मूल तत्त्व निष्पक्ष चिंतन एवं तर्क हैं। जीवन और जगत् के प्रति दृष्टिकोण में इस मूल भेद के कारण ही भक्त तथा दार्शनिक के विचारों एवं विश्वासों में आधारभूत अंतर पाया जाता है। स्पष्टतः इसका अर्थ यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों में संगति बनाए रखते हुए एक ही समय में तथा एक ही साथ भक्त और दार्शनिक नहीं हो सकता। यदि वह सच्चा भक्त या आस्थावान धर्मपरायण व्यक्ति है तो वह तो अथवा प्रमाणों की चिंता किए बिना केवल अपनी श्रद्धा से प्रेरित होकर अपने उपास्य विषय के प्रति आत्म-समर्पण करेगा; इसके विपरीत यदि वह वास्तव में दार्शनिक है तो वह आस्था और आराध्य विषय के अस्तित्व एवं स्वरूप के समर्थन में विश्वसनीय तथा पर्याप्त प्रमाणों की अनिवार्यतः खोज करेगा। ऐसी स्थिति में यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि एक ही व्यक्ति एक ही समय में तथा एक ही साथ भक्ति और दार्शनिक के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के कार्यों में आधारभूत अंतर है। इसी कारण यदि कोई व्यक्ति एक ही साथ भक्ति और दार्शनिक होने का दावा करता है तो उसके इस दावे को युक्तिसंगत नहीं माना जा सकता। वस्तुतः धर्म तथा दर्शन इन दोनों का दीर्घकालीन इतिहास इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही साथ सच्चा भक्त और सच्चा दार्शनिक नहीं हो सकता। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि धर्म और दर्शन दोनों मानव-जीवन के बहुत महत्त्वपूर्ण पक्ष होते हुए भी एक-दूसरे से मूलतः भिन्न हैं।
Disclaimer -- Hindiguider.com does not own this book, PDF Materials, Images, neither created nor scanned. We just provide the Images and PDF links already available on the internet or created by HindiGuider.com. If any way it violates the law or has any issues then kindly mail us: 24Hindiguider@gmail.com